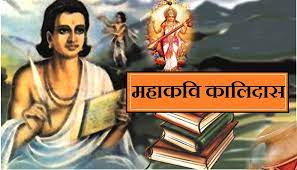मां काली के आशीर्वाद से विद्वान बने कालिदास, रच दी साहित्य की सर्वोत्तम कृतियां
डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्त्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। अभिज्ञानशाकुंतलम् कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य रचना मानी जाती है। मेघदूतम् कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की कल्पनाशक्ति और अभिव्यंजनावादभावाभिव्यन्जना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है और प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत रखंडकाव्ये से खंडकाव्य में दिखता है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और तदनुरूप वे अपनी अलंकार युक्त किन्तु सरल और मधुर भाषा के लिये विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके प्रकृति वर्णन अद्वितीय हैं और विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिये जाने जाते हैं। साहित्य में औदार्य गुण के प्रति कालिदास का विशेष प्रेम है और उन्होंने अपने शृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। कालिदास के परवर्ती कवि बाणभट्ट ने उनकी सूक्तियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है. रचनाएं छोटी-बड़ी कुल लगभग चालीस रचनाएँ हैं जिन्हें अलग-अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है।इनमें से मात्र सात ही ऐसी हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदासकृत मानि जाती हैं: तीन नाटक(रूपक): अभिज्ञान शाकुन्तलम्, विक्रमोर्वशीयम् और मालविकाग्निमित्रम्; दो महाकाव्य: रघुवंशम् और कुमारसंभवम्; और दो खण्डकाव्य: मेघदूतम् और ऋतुसंहार। इनमें भी ऋतुसंहार को प्रो॰ कीथ संदेह के साथ कालिदास की रचना स्वीकार करते हैं। नाटक मालविकाग्निमित्रम् कालिदास की पहली रचना है, जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती है। मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उसके प्रेम-संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुन्तलम् कालिदास की दूसरी रचना है जो उनकी जगतप्रसिद्धि का कारण बना। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन के अलावा दुनिया के अनेक भाषाओं में हुआ है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है जो वन में एक परित्यक्त ऋषि पुत्री शकुन्तला (विश्वामित्र और मेनका की बेटी) से प्रेम करने लगता है। दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आते हैं। इसी बीच ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप दे देते हैं कि जिसके वियोग में उसने ऋषि का अपमान किया वही उसे भूल जाएगा। काफी क्षमाप्रार्थना के बाद ऋषि ने शाप को थोड़ा नरम करते हुए कहा कि राजा की अंगूठी उन्हें दिखाते ही सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन राजधानी जाते हुए रास्ते में वह अंगूठी खो जाती है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है। शकुंतला लाख गिड़गिड़ाई लेकिन राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब एक मछुआरे ने वह अंगूठी दिखायी तो राजा को सब कुछ याद आया और राजा ने शकुंतला को अपना लिया। शकुंतला शृंगार रस से भरे सुंदर काव्यों का एक अनुपम नाटक है। कहा जाता है काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला (कविता के अनेक रूपों में अगर सबसे सुन्दर नाटक है तो नाटकों में सबसे अनुपम शकुन्तला है।) विक्रमोर्वशीयम् एक रहस्यों भरा नाटक है। इसमें पुरूरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। पुरूरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पुरूरवा से प्रेम के कारण वह वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। इससे इंद्र गुस्से में उसे शापित कर धरती पर भेज देते हैं। हालांकि, उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो वह फिर स्वर्ग लौट सकेगी। विक्रमोर्वशीयम् काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है। महाकाव्य कुमारसंभवम् उनके महाकाव्यों के नाम है। रघुवंशम् में सम्पूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएँ हैं, तो कुमारसंभवम् में शिव-पार्वती की प्रेमकथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। रघुवंशम् में कालिदास ने रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया है। खण्डकाव्य मेघदूतम् एक गीतिकाव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से सन्देश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बना कर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। मेघदूत के दो भाग हैं – पूर्वमेघ एवं उत्तरमेघ। ऋतुसंहारम् में सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अन्य रचनाएँ इनके अलावा कई छिटपुट रचनाओं का श्रेय कालिदास को दिया जाता है, लेकिन विद्वानों का मत है कि ये रचनाएं अन्य कवियों ने कालिदास के नाम से की। नाटककार और कवि के अलावा कालिदास ज्योतिष के भी विशेषज्ञ माने जाते हैं। उत्तर कालामृतम् नामक ज्योतिष पुस्तिका की रचना का श्रेय कालिदास को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काली देवी की पूजा से उन्हें ज्योतिष का ज्ञान मिला। इस पुस्तिका में की गई भविष्यवाणी सत्य साबित हुईं। श्रुतबोधम् शृंगार तिलकम् शृंगार रसाशतम् सेतुकाव्यम् पुष्पबाण विलासम् श्यामा दंडकम् ज्योतिर्विद्याभरणम् काव्य सौन्दर्य मुख्य लेख: कालिदास का काव्य सौन्दर्य कालिदास को कविकुलगुरु, कनिष्ठिकाधिष्ठित और कविताकामिनीविलास जैसी प्रशंसात्मक उपाधियाँ प्रदान की गयी हैं जो उनके काव्यगत विशिष्टताओं से अभिभूत होकर ही दी गयी हैं। कालिदास के काव्य की विशिष्टताओं का वर्णन निम्नवत किया जा सकता है: भाषागत विशिष्टताएँ कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और उन्होंने प्रसाद गुण से पूर्ण ललित शब्दयोजना का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का लक्षण है – “जो गुण मन में वैसे ही व्याप्त हो जाय जैसे सूखी ईंधन की लकड़ी में अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठती है” और कालिदास की भाषा की यही विशेषता है। कालिदास की भाषा मधुर नाद सुन्दरी से युक्त है और समासों का अल्पप्रयोग, पदों का समुचित स्थान पर निवेश, शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इत्यादि गुणों के कारण उसमें प्रवाह और प्रांजलता विद्यमान है। अलंकार योजना कालिदास ने शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है और उन्हें उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त और उनकी उपमाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। उदहारण के लिये: संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा। नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः।। अर्थात् स्वयंवर में बारी-बारी से प्रत्येक राजा के सामने गमन करती हुई इन्दुमती राजाओं के सामने से चलती हुई दीपशिखा की तरह लग रही थी जिसके आगे बढ़ जाने पर राजाओं का मुख विवर्ण (अस्वीकृत कर दिए जाने से अंधकारमय, मलिन) हो जाता था। अभिव्यंजना कालिदास की कविता की प्रमुख विशेषता है कि वह चित्रों के निर्माण में सबकुछ न कहकर भी अभिव्यंजना द्वारा पूरा चित्र खींच देते हैं। जैसे: एवं वादिनि देवर्शौ पार्श्वे पितुरधोमुखी। लीला कमल पत्राणि गणयामास पार्वती।। अर्थात् देवर्षि के द्वारा ऐसी (पार्वती के विवाह प्रस्ताव की) बात करने पर, पिता के समीप बैठी पार्वती ने सिर झुका कर हाथ में लिये कमल की पंखुड़ियों को गिनना शुरू कर दिया। कालिदास जी की रचनाओं की खास बातें कालिदास जी अपनी रचनाओं में अलंकार युक्त, सरल और मधुर भाषा का इस्तेमाल करते थे। अपनी रचनाओं में श्रंगार रस का भी बखूबी वर्णन किया है। कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में ऋतुओं की भी व्याख्या की है जो कि सराहनीय है। कालिदास जी के साहित्य में संगीत प्रमुख अंग रहा। संगीत के माध्यम से कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकाश डाला। कालिदास जी अपनी रचनाओं में आदर्शवादी परंपरा औऱ नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते थे। महाकवि कालिदास को राष्ट्रकवि की उपाधि दी जाती है। माना जाता है कि वह हिमालय से कन्याकुमारी तक की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित थे। उनके अनुभव का क्षेत्र व्यापक था। उनकी रचनाओं में तप को भव्यता प्रदान की गई है। उनकी भाषा सहज, सुंदर और सरल है।